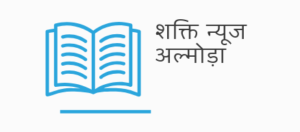Phool dev Shahni
Phool dev Shahniअपने पिता और दादा की तरह, फूल देव साहनी भी कभी 8 फीट गहरे (2.4 मीटर) कीचड़ भरे तालाबों में गोता लगाकर अपनी जीविका चलाते थे।
श्री शाहनी बताते हैं, “मैं प्रतिदिन घंटों 7 से 8 फीट पानी में गोता लगाता था और 8 से 10 मिनट बाद सांस लेने के लिए सतह पर आता था।”
उस गहरे अंधेरे में वह एक प्रकार के जल लिली के बीज इकट्ठा कर रहा था जिसे यूरीएल फेरोक्स कहा जाता था।
मखाना, फॉक्स नट्स या कमल के बीज के रूप में जाने जाने वाले ये बीज अपने पोषण मूल्य के लिए बेशकीमती हैं, क्योंकि इनमें विटामिन बी, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। उन्हें सुपरफूड के रूप में प्रचारित किया जा रहा है.
अक्सर नाश्ते के रूप में खाए जाने वाले मखानों का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में भी किया जाता है, जिसमें दूध की खीर भी शामिल है, साथ ही इसे आटे में भी पीसकर खाया जाता है।
उत्तर-पूर्वी भारतीय राज्य बिहार में, जहां श्री साहनी रहते हैं, विश्व का 90% मखाना उगाया जाता है।
लिली के पौधे की पत्तियाँ बड़ी और गोलाकार होती हैं और तालाब के ऊपर होती हैं। लेकिन बीज पानी के नीचे फली के रूप में बनते हैं और उन्हें इकट्ठा करना एक थका देने वाली प्रक्रिया थी।
श्री शाहनी कहते हैं, “जब हम नीचे गोता लगाते हैं, तो कीचड़ हमारे कान, आंख, नाक और मुंह में चला जाता है। इस वजह से हममें से कई लोगों को त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा, यह पौधा कांटों से ढका होता है, जिससे बीज इकट्ठा करते समय हमारे शरीर पर जगह-जगह कट लग जाते हैं।”
लेकिन हाल के वर्षों में किसानों ने खेती की प्रक्रिया बदल दी है। अब पौधे अक्सर उगाए जाते हैं खेतों में, बहुत उथले पानी में।
मात्र एक फुट पानी में बीज उगाकर श्री शाहनी एक दिन में दोगुना पैसा कमा सकते हैं।
“यह अभी भी कठिन काम है लेकिन मुझे अपनी परंपरा पर गर्व है। मेरे तीन बच्चे हैं और मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि मेरा एक बेटा मखाने के खेत में काम करने की विरासत को आगे बढ़ाए।”
 Madhubani Makhana
Madhubani Makhanaडॉ. मनोज कुमार मखाना की खेती में बदलाव लाने वालों में से एक हैं।
लगभग दस वर्ष पहले उन्हें यह अहसास हुआ कि गहरे तालाबों में इसकी खेती करना कठिन होगा।
वर्तमान में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र (एनआरसीएम) में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में, उन्होंने उथले पानी वाले खेतों में लिली की खेती को विकसित करने में मदद की।
पिछले चार या पांच वर्षों में यह तकनीक लोकप्रिय हो रही है।
“हमारे नवाचारों के साथ, मखाने की खेती अब जमीन पर उगाई जाने वाली किसी भी फसल की तरह आसान हो गई है। इसमें केवल एक फुट पानी की आवश्यकता होती है। श्रमिकों को गहरे पानी में घंटों काम नहीं करना पड़ता,” वे बताते हैं।
विभिन्न बीजों पर प्रयोग के बाद उनके केन्द्र को एक अधिक लचीली और अधिक उत्पादक किस्म मिली, जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे किसानों की आय तीन गुनी हो गई है।
डॉ. कुमार कहते हैं कि मखाना की खेती ने कुछ किसानों को हाल के वर्षों में बिहार में आई अनिश्चित मौसम की स्थिति और बाढ़ से निपटने में मदद की है।
अब एनआरसीएम ऐसी मशीनों पर काम कर रहा है जो बीजों की कटाई कर सकें।
इन सभी नवाचारों ने अधिक से अधिक किसानों को आकर्षित किया है।
2022 में, मखाने की खेती के लिए उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र 35,224 हेक्टेयर (87,000 एकड़) था, जो 10 वर्षों में लगभग तीन गुना वृद्धि है।
 Dhirendra Kumar
Dhirendra Kumarधीरेन्द्र कुमार उन किसानों में से एक हैं जिन्होंने हाल ही में मखाना की खेती शुरू की है।
हालाँकि वह एक खेत में पले-बढ़े थे, लेकिन वह अपने पिता के पदचिन्हों पर चलना नहीं चाहते थे।
“किसानों के रूप में हमने हमेशा गेहूं, मसूर और सरसों की खेती की, लेकिन हमें बहुत नुकसान हुआ।
वे कहते हैं, ”अधिकांशतः बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती हैं।”
पीएचडी की पढ़ाई के दौरान, वह मखाना की खेती पर काम कर रहे एक वैज्ञानिक के संपर्क में आये और उन्होंने अपने पारिवारिक खेत पर मखाना की फसल का प्रयोग करने का निर्णय लिया।
“परिणाम आश्चर्यजनक थे। पहले वर्ष में मैंने £340 का लाभ कमाया [US$432],” वह कहता है।
अब वह 17 एकड़ (6.9 हेक्टेयर) भूमि पर लिली उगाते हैं।
“मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मक्खी की खेती करूंगा, क्योंकि यह बहुत मेहनत वाला काम था, जिसे ज्यादातर मछुआरे ही करते थे।”
फसल में बदलाव से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुले हैं। श्री कुमार अब करीब 200 स्थानीय महिलाओं को रोजगार देते हैं जो बीज बोती हैं।
वे कहते हैं, “मेरा उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को रोजगार उपलब्ध कराना है ताकि वे कृषि में अनिश्चितता के कारण खेती न छोड़ दें।”
 Madhubani Makhana
Madhubani Makhanaऐसा नहीं है कि नवाचार सिर्फ इसी क्षेत्र में किए गए हैं।
मखाना के अग्रणी उत्पादकों में से एक होने के साथ-साथ, मधुबनी मखाना इसे दुनिया भर में निर्यात के लिए संसाधित करता है।
परंपरागत रूप से, मखानों की कटाई के बाद उन्हें धोया जाता है, भूना जाता है और फिर उन्हें फूटने के लिए एक हथौड़े जैसे औजार से मारा जाता है।
मधुबनी मखाना के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी शंभू प्रसाद कहते हैं, “यह विधि अपरिष्कृत, अस्वास्थ्यकर और जोखिम भरी है। यह श्रमसाध्य है, समय लेने वाली है और कई बार इससे चोट लगने और जलने की संभावना बढ़ जाती है।”
एनआरसीएम के साथ साझेदारी में उनकी कंपनी ने एक मशीन विकसित की है जो मखाने के बीजों को भूनकर उन्हें काटती है।
श्री प्रसाद कहते हैं, “इससे हमें मखाने की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है।”
इनमें से तीन मशीनें उत्तरी बिहार के मधुबनी स्थित उनके विनिर्माण संयंत्र में स्थापित की गई हैं।
यद्यपि मखाना की खेती और प्रसंस्करण में नवाचार से उत्पादन में वृद्धि हो रही है, लेकिन श्री प्रसाद को नहीं लगता कि यह कीमतों में गिरावट लाने के लिए पर्याप्त होगा।
वे कहते हैं, “मखाना की बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए, कीमतों में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि आवश्यक होगी।”
अपने खेत पर लौटकर धीरेन्द्र कुमार को लगता है कि मखाना की खेती दूरगामी बदलाव लाएगी।
वे कहते हैं, “जहां तक मखाने की फसल की बात है तो यह बिहार में नवाचार की शुरुआत है। यह राज्य का परिदृश्य बदल देगा।”